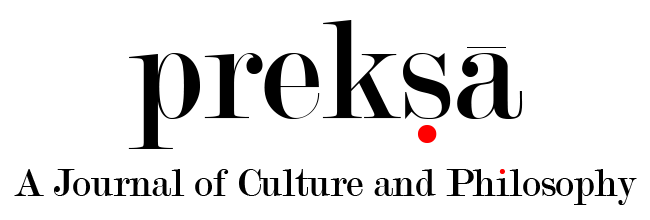अप्रतिम योद्धा महाराजा रणजीत सिंह
सिखों के योद्धाओं की परम्परा में महाराजा रणजीत सिंह का नाम भी श्रेष्ठतम योद्धाओं में लिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने ही उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (अफगानिस्तान और उसका निकटवर्ती क्षेत्र) में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्रिटिश लोगों के लिए वह एक बड़ी चुनौती बन गये थे। 13 नवम्बर 1780 में जन्मे रणजीत सिंह की एक आंख बचपन में चेचक के कारण नष्ट हो गई थी। उनके व्यक्तित्व की तेजस्वि...

उन्हे इस्लाम धर्म स्वीकरा करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। उस समय वहाँ उपस्थित काजी ने कहा कि गोविंद सिंह चूंकि हमारा शत्रु है इसके लिए इन बच्चों को सजा न दी जावे। परन्तु इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के अपराध में उन्हे जिंदा ही दीवार में चुनवा कर निर्दयता पूर्वक मार दिया गया। इन बच्चों को खडा कर उसके आसपास तीन फुट मोटी ईट व चूने की दीवार बनवा दी गई। उस समय बडे भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू देख कर छोटे भाई फतेह सिंह ने पूछा कि क्या आप डर के का...

गुरु तेग बहादुर का शौर्य
औरंगजेब ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां के सभी पंडितों की हत्या करने का प्रयास किया, मृत्यु के भय से उन्होंने कश्मीर नरेश को अपना राज्य समर्पित कर देने को कहा। इस प्रकार बिना विरोध कश्मीर इस्लाम के अधीन आ गया। चूंकि कश्मीरी पंडितों ने त्याग और बलिदान से मुंह मोड़ लिया इस कारण से पूरा प्रदेश इस्लाम की हत्यारी रीति का शिकार बन गया। औरंगजेब ने अपने सूबेदार शेर अफगन को इस संदेश के साथ कश्मीर भेजा कि या तो पंडित लोग इस्लाम स्वीका...

प्रतिष्ठा से वंचित सम्राट – हेमचन्द्र विक्रमादित्य
भारत के लम्बे इतिहास में कुछ युद्ध बडे निर्णायक सिद्ध हुई। पानीपत की तीनो लड़ाइयां इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। यदि इन लडाइयों के परिणामों में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाता तो भारत का भविष्य पूर्णतः बदल जाता। ऐसी ही एक लड़ाई में मारा गया महान योद्धा हेमू अर्थात हेमचन्द्र विक्रमादित्य था।
दो शताब्दियों तक दिल्ली पर इस्लामिक सल्तनत के बाद सनातन धर्म को दिल्ली के शासन पर पुनः स्थापित कर पाने का श्रे...

अजेय सम्राट : छत्रसाल
अतुलनीय शौर्य का एक और उदाहरण बुंदेलखंड का सम्राट छत्रसाल है। इसके कारण औरंगजेब तक भयभीत था। बुंदेलखंड का नाम उस क्षेत्र की देवी विंध्यवासिनी से मिला है। लोक कथा के अनुसार वहां के शासक ने अपनी सारी संपदा अपने पांचवें पुत्र पंचम को सौंप दी थी, इससे क्रोधित हो कर उसके शेष चारो भाइयों ने मिलकर पंचम से राज्य छीन लिया। तब पंचम ने विंध्याचल स्थित एक शक्ति पीठ देवी विंध्यवासिनी की उपासना की और जब वह देवी को अपने प्राणों की बलि देन...

राणा प्रतापसिंह की सफलता और उपलब्धियॉ उसकी नीतियों की योग्यता और प्रभाव को सिद्ध करती है। अपने बाहर वर्षों के सतत प्रयासों के पश्चात भी अकबर उससे कुछ भी छीन सकने में सफल नहीं हो सका। राणा प्रताप ने अपने पिता से प्राप्त राज्य को बिना क्षति अपने पुत्र को सौंपा था। यदि प्रतापसिंह अकबर के समक्ष समर्पण कर देता तो उसका पुत्र अकबर के दरबार में एक सामान्य स्थिति को ही प्राप्त कर पाता। बाद की घटनाओं ने प्रतापसिंह की समस्त उपलब्धियों को लील लिया।
राणा प्...

महाराणा प्रतापसिंह : एक अद्वितीय योद्धा
महाराणा प्रतापसिंह (महाराणा प्रताप) भारत के क्षात्र भाव के सबसे अधिक चमकीले हीरे है। वे उदयसिंह के तेईस (23) बच्चो में सबसे बडे थे। वह सिसोदिया वंश के योद्धा कुल में कुंभल गढ़ में जन्में थे। ‘एकलिंग स्वामी’ इनके परिवार के कुल देवता थे। अपने बचपन से ही उनमें महान योद्धा बनने के लक्षण दिखलाई देते थे। सन् 1572 में उदयसिंह की मृत्यु के उपरांत उसकी सबसे छोटी रानी का बेटा जगमल शासनासीन हुआ किंतु प्रजाजनों के भार...

मेवाड़ के महा क्षत्रिय
राजपूतों में संभवतः मेवाड़ का राजवंश श्रेष्ठतम है। मेवाड़ का केंद्र चित्रकूट (चित्तौड़) है। ऐसा प्रतीत होता है मानों एक बहुत बडे समतल भूभाग पर एक पहाड़ अचानक खड़ा हो गया है। इस पर्वत शिखर तथा उसके आसपास तक फैला अभेद्य किला चित्तौड़ का केंद्र स्थान है। यह मात्र सामरिक किला ही नहीं है किंतु यहां अत्यंत मनोहारी शिल्प कृतियों का भंडार भी है। यहीं पर भोज द्वारा निर्मित महादेव मंदिर तथा मीराबाई द्वारा निर्मित कृष्ण मंदिर भी है।...

मध्य भारतीय मुस्लिम साम्राज्य जैसे अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुण्डा, बीजापुर, गुलबर्गा आदि सतत रूप से लड रहे थे जिसमें यदाकदा विजयनगर का राजा किसी भी एक मुस्लिम राज्य का पक्षधर हो जाता था। इतिहासकारों के अनुसार रामराय ऐसे राजनैतिक दांवपेच किया करता था जो उसका एक कूटनीतिक हथियार था, किंतु जब उसके संबंध पुर्तगालियों से खराब हुए और उसे उसके विरुद्ध कूटनीतिक असफलता प्राप्त हुई तो उसने उन्हें युद्ध में हराते हुए उनके एक लाख पैगोडा छीन लिए। यद्यपि वह शक...

भारतीय विद्या भवन द्वारा इतिहास के अनेक खण्ड ग्रंथ भारतीय इतिहास के सत्य को दर्शाने हेतु प्रकाशित हुए है। आर. सी. मजूमदार लिखते है -
सम्पादक का यह प्रयास रहेगा कि वह तीन सिद्धांतों का पालन कर सकें – इतिहास किसी व्यक्ति या समुदाय के सम्मानार्थ नहीं है, इसका लक्ष्य सत्य का वह प्रस्तुतिकरण है जो इतिहासकारों द्वारा मान्य ठोस मानकों पर आधारित हो और तीसरा बिना डर, द्वेष, दुर्भावना, पूर्वाग्रह, या भावावेश, राजनैतिक अथवा मानवीय, अतिरिक्त प्रभावों से...